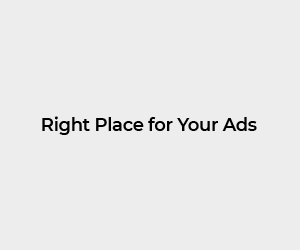गाजीपुर । एक सम्पूर्ण व्यावहारिक जीवन दर्शन को समेटे हुए ग्रन्थ के रूप में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस पर जितनी भी चर्चा, आलोचना-समालोचना और समीक्षा हुई है उतनी शायद ही किसी अन्य लिपिबद्ध ग्रन्थ की हुई होगी, और हो भी क्यों न? ऐसा और कौन सा ग्रन्थ है, जिसने हम संसारी जीवों के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राजनैतिक जीवन के विभिन्न अंगों को इतने मर्मस्पर्शी एवं स्पष्ट ढंग से छुआ हो। चाहे वह परिवार के सदस्यों के परस्पर संबंधों की गरिमा-मर्यादा हो, समाज के विभिन्न वर्गों के आपसी संबंधों की मर्यादा हो अथवा राजकीय काम-काज व राजा के कर्तव्यों की।श्री रामचरितमानस में निरूपित जीवन-व्यवस्था एक आदर्श समाज एवं आदर्श राज्य की कोरी कल्पना मात्र न होकर पूर्णतः अनुभवगम्य और व्यावहारिक है। इस ग्रन्थ के माध्यम से गोस्वामी जी ने परस्पर स्नेह-सम्मान के साथ कर्त्तव्य-परायणता के माध्यम से न केवल जीवन को समृद्ध-सुखी बनाने में असंख्य-अप्रतिम योगदान दिया है वरन मानस के पात्रों के माध्यम से ढेरों सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में अभूतपूर्व कार्य किया है। आज के सन्दर्भ में हमारे समक्ष विद्यमान विशालतम चुनौतियों में जो अग्रणी हैं उनमें सामाजिक व्यवस्था में समरसता का उत्तरोत्तर ह्रास प्रमुख है। स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि इक्कीसवीं सदी के तेईस वर्ष और भारतीय संविधान लागू होने के तिहत्तर वर्ष बाद भी वर्ण-व्यवस्था और रुढ़ियों के कुचक्र को भेदने में सफल होने की अपेक्षा हम उसमें और उलझते जा रहे हैं और अपने वर्तमान को संभालने के संकट से जूझ रहे हैं।
सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता-अखंडता के लिए रामचरित मानस ने जो योगदान कई सौ वर्ष पूर्व किया था वह आज भी उतना ही नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक प्रासंगिक तथा आवश्यक है।मानस के रचना काल को देखें तो पता चलता है कि उस समय वर्ण-व्यवस्था के अतिरिक्त भारतीय समाज मुख्यतः दो सम्प्रदायों – वैष्णव और शैव – में विभाजित था। तत्कालीन अन्य वैश्विक धर्मों के मतावलम्बियों में विभाजित समूहों-अनुयायियों की भांति, हिन्दू धर्म के अनुयायी भी दो वर्गों में विभक्त थे और अपने पंथ (वैष्णव-शैव) तथा आराध्य (भगवान श्री राम एवं भगवान शंकर) को एक-दूसरे से अधिक समझने की वजह से प्रायः एक-दूसरे से विद्वेष-विद्रोह में अपना समय व ऊर्जा व्यर्थ करते थे जिसके फलस्वरूप हानि अंततः समाज की होती थी।कोई भी साहित्यकार समाज का पारखी होता है, समाज की दिशा-दशा पर दृष्टि रखता है तथा अपनी लेखनी के माध्यम से कुरीतियों का शमन करने और समाज के उत्थान में अपनी भूमिका निभाता है। निश्चित रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के माध्यम से तत्कालीन समाज को इस सांप्रदायिक विभाजन के फलस्वरूप होने वाली हानि से उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। भगवान के दोनों स्वरूपों (भगवान शंकर एवं भगवान श्री राम) को एक दूसरे का उपासक बताकर, एक-दूसरे के प्रति सम्मान दिखाकर उनके अवलम्बियों-उपासकों के परस्पर द्वन्द को निर्मूल कर दिया।बालकाण्ड में वर्णित प्रयागराज के मुनि-समागम में ऋषि भरद्वाज अपनी जिज्ञासा की शांति हेतु ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ अपने संवाद में भगवान शंकर को भगवान श्रीराम का उपासक बताते हुए कहते हैं कि हर कोई अविनाशी भोलेनाथ की उपासना करता है, वहीँ स्वयं भगवान शंकर श्री राम की महिमा का बखान करते हैं –
“संतत जपत संभु अविनासी, सिव भगवान ज्ञान गुन रासी।
सोपि राम महिमा मुनिराया, सिव उपदेश कीन्ह करि दाया।
इसके पश्चात् –
“सम्भु समय तेहि रामहिं देखा, उपजा हियँ अति हरष विसेषा
तिन्ह नृपसुतहिं कीन्ह परनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा।।
तथा “जासु कथा कुम्भज ऋषि गाई… सोइ मम इष्ट देव रघुबीरा…” के माध्यम से बार-बार शंकर का राम के प्रति सम्मान दिखाना निश्चित ही शैवों के मन से वैष्णवों के प्रति विद्वेष भाव समाप्त करने और दोनो सम्प्रदायों के बीच की खाई को भरने और उनमे परस्पर सौहार्द स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया अत्यावश्यक, सार्थक, सफल प्रयास था ।यही नहीं बालकांड में माता पार्वती को श्री राम जन्म-प्रसंग की कथा सुनाते हुए भगवान शंकर जन्मोत्सव का आनंद देखने के लिए कागभुशुण्डि के साथ मनुष्य रूप में चोरी से अपने अयोध्या विचरण तथा बाल-लीला देखने की चर्चा करते हैं, जिससे उनके मन में भगवान राम के प्रति आदर परिलक्षित होता है। यथा-औरउ एक कहउँ निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी।कागभुशुण्डि संग हम दोऊ, मनुज रूप जानइ नहि कोऊ। परमानन्द प्रेम सुख फूले, वीथिन्ह फिरहि मगन मन भूले। विचित्रता यह कि ये प्रेम-सम्मान एकांगी नहीं बल्कि विशुद्ध द्विपक्षी है। इसकी एक अति मनोहारी झलक पुष्प वाटिका में मिलती है जब सीताजी शंकर-प्रिया भवानी से अपने लिए एक सुयोग्य वर की प्रार्थना करती हैं- गयीं भवानी भवन बहोरी, बंदि चरन बोली कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी।और धनुष यज्ञ के समय जब पिनाक-भंजन हेतु श्री राम की सुकुमार काया और शिव-धनुष की विशालता का अनुमान लगाकर मन में किंचित चिंतित-विचलित होती हैं और माँ भवानी और भगवान भोलेनाथ को याद करती हैं –मन ही मन मनाव अकुलानी, होहु प्रसन्न महेस भवानी।करहु सफल आपनि सेवकाई, करि हितु हरहु चाप गरुआई ।यदि हम थोड़ी और गहराई में उतरें तो पायेंगे शंकर और राम (अर्थात शैव-वैष्णव) समीकरण-एकीकरण मानस का छिटपुट प्रसंग न होकर यत्र-तत्र-सर्वत्र का प्रसंग है। इसका प्रमाण हमें इस तथ्य से मिलता है कि श्री राम-शंकर का परस्पर स्नेह-सम्मान, पूजा-अर्चना बालकांड से प्रारम्भ होकर अयोध्याकांड और लंकाकांड होते हुए उत्तरकांड तक बारहमासी पवित्र सलिला सदृश निरंतर चलती रहती है। वनगमन-प्रसंग में भी श्रीराम अपने चौदह-वर्षीय वनवास की यात्रा पर अयोध्या से प्रस्थान करते समय विघ्नहर्ता गणेश और माँ भवानी के साथ भगवान शंकर का ही स्मरण करते हैं –“गणपति गौरि गिरीसु मनाई, चले असीस पाई रघुराई”। और गंगा जी को पार करने के बाद पुनः शंकर को शीश झुका कर वनगमन करते हैं –
“तब गणपति सिव सुमिरि प्रभु, नाइ सुरसरिहि माथ।
सखा अनुज सिय सहित वन, गवन कीन्ह रघुनाथ।“
लंका विजय हेतु सेतु बंधन के समय जब परंपरानुसार पूजा की बात आती है तो भगवान राम कहते हैं –
“करिहउँ इहां संभु थापना, मोरे ह्रदय परम कल्पना।
लिंग थापि विधिवत करि पूजा, सिव समान प्रिय मोहि न दूजा।सिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेहुँ नहि पावा।संकर विमुख भगति चह मोरी, सो नारकी मूढ़ मति थोरी। संकर प्रिय मम द्रोही, सिव द्रोही मम दास।
सो नर करहिं कल्प भरि, घोर नरक माह बास।“
राम से ऐसा कहलवाकर तुलसी दास जी वैष्णवों को भी शैवों के प्रति वैर-वैमनस्य छोड़कर उन्हें मैत्री भाव हेतु प्रेरित ही नहीं बल्कि विवश करते हैं । कितना अद्भुत और सुखद है कि यह क्रम सेतुबंध के साथ यहीं समाप्त न होकर लंका-विजय तक चलता है जब समस्त देवताओं द्वारा की गयी प्रार्थना के क्रम में भगवान शंकर आते हैं और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर, कमल-नयन समान नेत्रों में जल भरकर, पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव विनती करते हुए कहते हैं –“मामभिरक्षय रघुकुल नायक, धृत वर चाप रुचिर कर सायक। अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उर अंतर।“ इसके साथ यह कहकर जाते हैं कि-“नाथ जबहि कौशल पुरी होइहि तिलक तुम्हार,
कृपासिंधु मैं आउब देखन चरित तुम्हार।“
और अयोध्या आने के बाद जब श्रीराम-राज्याभिषेक होता है तो पुनः शंकर जी का आगमन होता है –
“बैनतेय सुनु संभु तहँ आये जहँ रघुबीर,
बिनय करत गद्गद गिरा बोले पुलक सरीर।
जय राम रमा रमनं समनं भवताप भयाकुल पाहि जनम…।“
और अंत में – “बरनि उमापति रामगुन हरखि गए कैलास।“
यह तो रही पंथ अथवा संप्रदाय-आधारित राष्ट्रीय-एकता में मानस के योगदान की बात। अब बात करते हैं सामाजिक समरसता की –
यदि हम सामाजिक समरसता की दृष्टि से देखें तो वहां भी रामचरित मानस हमें प्रतिबिम्ब और पथ दोनों दिखाता है। प्रतिबिम्ब इसलिए कि हम अपने व्यक्तित्व एवं तदनुरूप कार्य व्यवहार व सामाजिक योगदान के वास्तविक रूप को जान सकें, और पथ इसलिए कि जहाँ हम एक समाज के रूप में भटक रहे हैं वहां सन्मार्ग का चयन कर सकें और उस पर चलने का साहस-सामर्थ्य जुटा सकें।
इसी क्रम में श्रीराम को मना कर वापस ले जाने के लिए के लिए चित्रकूट जाते हुए भरत की भेंट निषादराज से होती है तो इस समरसता और मर्यादा का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है जब निषाद अपना नाम बताता है-
“देखि दूरी ते कहि निज नामू….” (बताने के लिए कि मैं नीची जाति का हूँ), और इस पर भरत की प्रतिक्रिया इस समरसता का प्रमाण देती है जब वह अपना रथ त्याग कर बड़े प्रेम से उसकी ओर जाते हैं –“राम सखा सुनि स्यंदन त्यागा, चले उतरि उमगत अनुरागा। करत निषाद दंडवत पाई, प्रेमहि भरत लीन्ह उर लाई। भेंटत भरत ताहि अति प्रीती, लोग सिहाहिं प्रेम कइ रीती।“ और इसकी अप्रत्याशित पराकाष्ठा तो तब होती है जब चित्रकूट में निषाद नीची जाति का होने के कारण डर व् संकोच वश दूर से प्रणाम करता है और मुनि वशिष्ठ (ब्राह्मण होने के नाते जिनसे अधिक ऊंचा व् प्रतिष्ठित होने की उस समय कल्पना नहीं की जा सकती) निषादराज को अपने बाहुपाश में भर कर मिलते हैं –
“प्रेम पुलक केवट कहि नामू कीन्ह दूरि ते दंड प्रनामू,
रामसखा ऋषि बरबस भेंटा जिमि महि लुठत सनेह समेता।“ मानस में वर्णित यह सामाजिक सद्भाव यहीं तक – अर्थात निषाद (आज के सामाजिक सन्दर्भों में तथाकथित अनुसूचित जाति) तक सीमित नहीं रहता। इसके आगे श्रीरामचरितमानस जनजाति को भी समाज का अभिन्न और सम्मानित अंग बनाता है जब गोस्वामी तुलसीदास जी श्री हनुमान जी के माध्यम से वानरराज सुग्रीव की भेंट भगवान राम से करवाते हैं। किसी ने वानर को वन में रहने वाला नर कहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि सुग्रीव और उनकी सेना के सदस्य वानर-भालू ही न होकर जंगल में रहने वाली जातियां रही होंगी जो कि नगर और गांव में रहने वालों से कम ‘शिक्षित-सभ्य’ मानी जाती रही होंगी (यद्यपि शिक्षा की दृष्टि से हनुमान जी को इस श्रेणी में रखना अनुचित होगा)। किष्किंधा में राम-लक्ष्मण से भेंट होने पर हनुमान जी अपने राजा सुग्रीव का परिचय देकर उनके साथ मित्रता का निवेदन करते हैं – “नाथ शैल पर कपि पति रहई, ……तेहि संग नाथ मयत्री कीजै।“मानस में किष्किंधाकांड का प्रसंग रखने की पृष्ठभूमि में गोस्वामी जी के मन में केवल मित्रता मात्र का वर्णन करना नहीं था वरन इसके माध्यम से वह यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि राजा (शासक) को किसी बड़े काम की सफलता के लिए (चाहे वह शत्रु-विजय हो अथवा कोई अन्य बड़ा सामाजिक-राष्ट्रव्यापी अभियान), जन- सहभागिता (सबके विकास के लिए सबका साथ) परम आवश्यक है। मानस के उपर्युक्त प्रसंग इस बात की पर्याप्त पुष्टि करते हैं कि समरसता (सोशल हारमनी) के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण (नेशनल इंटीग्रेशन) रामचरितमानस का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है।डा. त्रिवेणी सिंह, प्राचार्य, बापू महाविद्यालय सादात गाजीपुर
Leave a comment